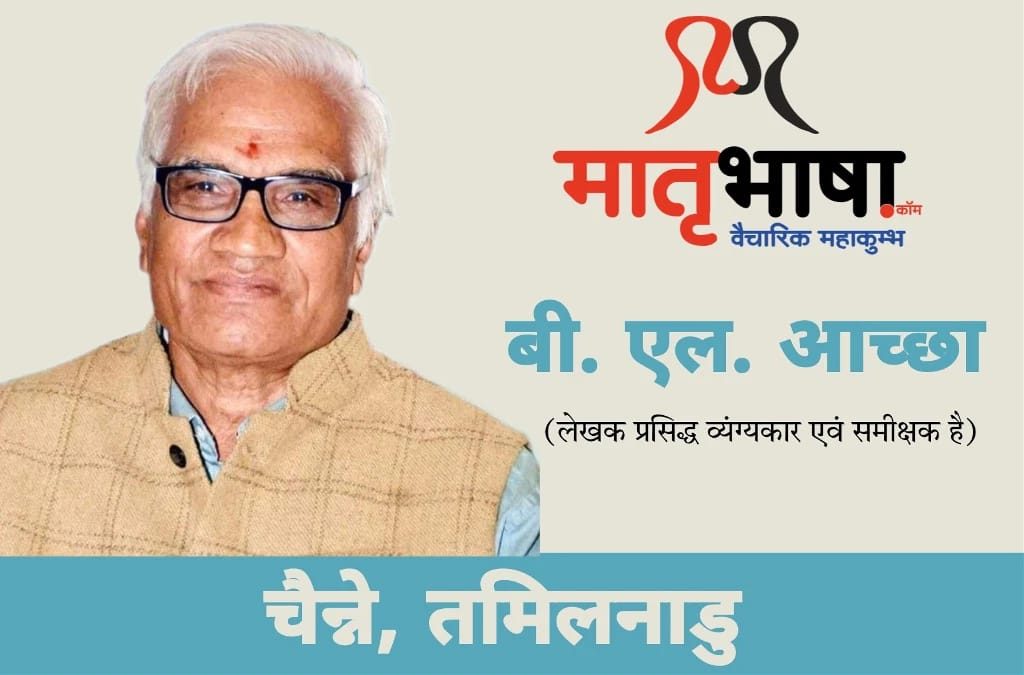
व्यंग्य
मॉर्निंग वॉक के वे आदी हैं। कोहरे की परत वाली ठंड में भी वे आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह लदे चले आए। बोले- ‘निकलो भी रजाई से।’ मैंने कहा- ‘इस बार तो ठंड बर्फानी-सी है। बिस्तरस्थ रहना ही बेहतर है।’ शरीर पर तीन-चार गरम कपड़े, सिर पर मोटा-सा टोपा और गले में निहायत गरम मफ़लर डाले, वे दबी ज़ुबान में बोले- ‘अरे, ठंड क्या है, चलोगे तो गर्मी आ जाएगी।’ मैंने भी अपना फुल स्वेटर पहना। पीटी शू बाँधे और दरवाज़ा बंद किया।
चलते-चलते अख़बार दिख गया। बॉक्स न्यूज़ पर नज़र चली गई- ‘शाजापुर में प्रदेश का न्यूनतम तापमान।’ अभी तक गर्म था। पढ़ते ही ठंड लगने लगी। उनकी आर्मस्ट्रॉन्ग की सी वेशभूषा के आगे मेरा इकलौता स्वेटर ठंड की अख़बारी दहशत को सह नहीं पा रहा था।
रास्ते में वे बोले- ‘सुहानी ऋतु तो शरद ही है। दिनभर सूट लादो। बदल-बदल कर पहनो। पत्नी के साथ निकलो तो तरह-तरह की शालों-कार्डिगनों के साथ। जूते और मौजों में तो पैर भी कुनकुने लगते हैं। खाने-पीने का मज़ा ही ठंड का है। फिर दिखने में मैं भले ही विदेशी लगूं, मगर खाने में ठेठ देसी उड़द के लड्डु, मूंग की बर्फी, तरह-तरह के हलवे। अच्छा-सा सूखा मेवा डाल दो। ज़रा-सी केशर कस्तूरी। फिर क्या, ठंड भी ख़ुद ही गरमा जाती है।’
इन सारी बातों से मेरी आंतों को ठंड लगने लगी। इकलौती जर्सी भी ठंडाने लगी। मगर उनकी गर्माहट तो लहक-सी रही थी। मैंने भी तय किया, सूट तो सिलवा ही लिया जाए। मगर मध्यमवर्गीय बजट ने कतरब्योंत स्वीकार न की, बहुत दबाव के बाद पत्नी ने कहा- ‘देखो जी, एक सूट तो तीन-चार हज़ार का पड़ेगा। फिर भी रहेगा तो एक ही न? उससे अमीरी तो नहीं झलकने वाली, मैं सात स्वेटर बना देती हूँ। रोज़ बदल-बदल कर जाओगे, तो लोगों की नज़रें तो टिकेंगी ही।’ एक क्लासिक सूट के बदले सात रंगीन स्वेटर मुकाबला न भी हो, पर भी जेब इससे आगे बढ़ न सकी।
अब हर दिन और हर ग्रह के रंग में मैच करते ये स्वेटर पहनकर निकलता हूँ, तब पुराने दिन याद आ जाते हैं। वह भी कैसी ठंड थी! सर्दीले तालाबों में कमल खिला करते थे और मेरा सर्दीला बदन इकलौते स्वेटर में। अब तालाबों के कमल गायब हैं और मैं रोज़-रोज़ नए रंग के स्वेटर में खिलता हुआ सड़क पर निकलता हूँ, तब एरियल घुले बगुले आकाश में पंगतवार उड़ते थे, अब मैं भी उसी बगुला स्वेटर को पहने सड़क पर उड़ान भरता हूँ। मगर स्वेटर पहनते-पहनते श्रीमतीजी टोक रही हैं- ‘जब नया फुल स्वेटर पहने हो तो शर्ट ज़रा पुरानी ही धका लो। बस, कॉलर ज़रा ठीकठाक हो।’ मुझे मालूम है कि नए जूतों में मैंने फटे हुए मौजों से काम धकाया और नई-सी सफ़ारी के नीचे बदन झाँकते बनियान से भी। बेहद ज़रूरी होने पर भी उन्हें उतारा नहीं है। फिर भी नये स्वेटर में जंच-संवर कर निकलने के सुपर क्लास उच्छाह को श्रीमतीजी ने मेरी मझौली औकात पर लाकर खड़ा कर दिया है।
शेक्सपियर ने तो कह दिया- ‘जो कुछ चमकता है, सोना नहीं होता।’ क्या मैं भी सूक्ति बनाऊँ- ‘हर नये पुल स्वेटर के नीचे नया शर्ट नहीं होता। (बल्कि ठीकठाक कॉलर बाला घिसा-पुराना शर्ट ही होता है)। ऐसी हालत में श्रीमतीजी से कहते नहीं बन रहा, उड़द के मेवा डले लड्डू या मूँग की बर्फी के लिए। संभव है घर की वित्तमंत्री ‘तोप माँगे-तमंचा मिले’ की तर्ज पर कह दें- ‘अजी गुड़ मूँगफली की चिक्की बेहद स्वादिष्ट होती है। ये बादाम-काजू तो चोंचले हैं।’
और रात को भी उसी आर्मस्ट्रॉन्गनुमा मित्र के साथ टहलने को निकला हूँ। उनकी वेशभूषा तो यों भी सर्दी को टक्कर मारती है। चलते हुए कह रहे हैं- ‘सरकार भी बेहद शोषण करती है। भत्ता रिलीज़ नहीं कर रही है। कार के पेट्रोल पर सीलिंग लगा दी है। अभी इन्कम टैक्स के मारे तो दिसंबर-जनवरी में ही इकतीस मार्च नज़र आ रहा है। तभी उनकी नज़र सड़क किनारे कुछ मज़दूर-मामाओं के डेरों पर पड़ी। कई चूल्हे जल रहे थे। मकई की रोटियाँ सिक रही थीं। इस सिकती हुई गंध को भीतर भरते हुए वे बोले- ‘यार ज़िंदगी तो इनकी है। मोटा-सा टिक्कड़ बनाया और खा लिया। न सरकार की परवाह, न टैक्स की। यहीं रात को गुदड़ी में सो पड़े रहेंगे। इनकी भी अपनी मस्ती है।’
मन में आया, कह दूँ- ‘हुज़ूर, मुबारक हो आपको यह मस्ती।’ मुझे याद है एक बार रेल यात्रा में बर्थ तो मिल गई, मगर ओढ़ने-बिछाने का कुछ न था। सो मारे सर्दी के पाँव तक पसारे न गए। बैठे-बैठे ही रात गुज़ारी उस ठंड में । अब कई मकानों मंज़िलों का निर्माता यह झाबुआ का आदिवासी मामा इस सर्दीले आसमां के नीचे गुदड़ी में सिकुड़ कर सो रहा है। मगर सूखा मेवा डले उड़द के लड्डू का स्वाद, इस मामा की मकई की रोटी की सिकती हुई गंध को भी अपने कब्जे में कर रहा है। अपने इस सुपर क्लास मित्र की गर्माती हुई ठंडक और इस आदिवासी मामा की आकाश तले ठंडाती हुई गुदड़ी के बीच कैसे कहूँ- ‘आई शरद सुहावनी’।
#बी.एल.आच्छा
वरिष्ठ समीक्षक एवं व्यंग्यकार,
चैन्ने, तमिलनाडु


