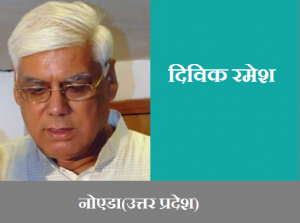
बात पहले की है । भारतीय मिथकीय पात्र और लेखिकाओं का नारी विमर्श में डूबा हुआ था। यूं मेरे पास, उससे भी बहुत पहले, अपने काव्य नाटक ’खण्ड खण्ड अग्नि’ के सिलसिले में वाल्मीकि रामायण के अग्नि परीक्षा-प्रसंग की सीता का अपने समय के लिहाज से सशक्त नारी विमर्श भी पूर्वपीठिका के रूप में सामने था। हिन्दी की जिन लेखिकाओं के विचारों और रचनाओं से परिचित था उनकी ओर भी ध्यान गया। मैंने हमेशा से निर्मला जैन, कृष्णा सोबती मन्नू भण्डारी, मृदला गर्ग, चित्रा मुद्गल जैसी लेखिकाओं के निजी जीवन, चिन्तन और रचनागत व्यवहार में नारी -विमर्श का एकांगी नहीं अपितु सर्वांगीण, संतुलित एवं सटीक पाठ पाया है । जब चित्रा जी का आवां पढ़ने का अवसर मिला तो उनके प्रति मेरी धारणा और भी अधिक पुख्ता हो गई और कहीं प्रसंगवश उसे अपने एक लेख में प्रकट भी किया। आज थोड़ा विस्तार में जाने का मन है। ठहरिए, पहले अपने अब तक अनुभव के बलबूते यह भी बता दूं कि नारी की अस्मिता और उसके सशक्तीकरण संबंधी अपने विचारों और चिन्तन में स्पष्ट और मजबूत चित्रा जी आपसी व्यवहार में मनुष्योचित मृदुता और शालीनता को कभी नहीं छोड़तीं। मैंने उन्हें एक पत्नी के रूप में अपने अशक्त होते गए पति (पुरुष के जिस रूप पर नारी विमर्श सबसे अधिक घटता नजर आता है ) के साथ हमेशा पूरी तरह मन से खड़ा पाया है । अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरुष के अन्य रूपों के साथ भी वे ऐसी ही खड़ी मिलती होंगी। उनके समक्ष प्रतिरोध और प्रतिशोध की संकल्पनाएं पारदर्शी हैं । इस संदर्भ को फिलहाल यहीं छोड़ता हूं।
बहुत सोच-विचार के बाए मुझे, हिन्दी साहित्य में जो भी विमर्श चल रहे हैं उनमें ’प्रतिरोध’ की राह उचित लगती है ।प्रताड़ित एवं पददलित मनुष्य के जीवन में प्रतिशोध, भाव के रूप में कितना ही तात्कालिक और स्वाभाविक भी क्यों न हो लेकिन राह के रूप में उपयुक्त नहीं लगता। किसी को कॆसा होना चाहिए उस रूप में ढालने के लिए प्रतिरोध ही प्रतिशोध की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध हुआ करता है और दर्शन की भूमिका तक पहुंचने के योग्य हो जाया करता है । बात को नारी विमर्श के एक प्रमुख आयाम ’देह मुक्ति’ के संदर्भ से समझी जा सकती है । नारी-विमर्श और देह-विमर्श का चोली-दामन का साथ माना गया है। देह मुक्ति की बात कही और समझी जा रही है । बहस यह भी है कि देह मुक्ति वस्तुत: देह से परे जाना है । देह से परे जाना क्या है ? मान लो एक स्त्री का बलात्कार होता है । स्पष्ट है कि पुरुष (बलात्कारी) दोषी है । लेकिन एक सोच के अनुसार दाग स्त्री की देह को लगता रहा है । एक और उदाहरण लीजिए । भारतीय संदर्भ में । दो प्रेमी हैं । उनके देह संबंध स्थापित हो गए । किसी कारण विवाह नहीं हुआ । अब लड़की को प्राय: यह सलाह दी जाती है कि वह अपने देह-संबंध को छिपाए । नहीं छिपाएगी तो ,यौन शुचिता के हिमायती होने के कारण पुरुषों से ताने सुनती रहेगी । अपवित्र कहलाएगी । ऐसे में देह मुक्त अनिवार्य हो जाती है और देह से परे जाने का अर्थ भी समझ में आता है -अर्थात सारी पवित्रता, शुचिता आदि का ठेका देह से जोड़ देने वाली सोच का विरोध । लेकिन स्त्री देह का ऎसा उपयोग जो मेनका का विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए किया गया था उसकी विडम्बना को गहराई से समझना होगा । ऐसी स्थिति में मेनका का विद्रोह मुखरित होना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि उसकी देह को अपवित्र करने की साजिश की वह शिकार हुई है । इस संदर्भ में देह का क्या बिगड़ता है कह कर पुरुष को क्षमा या उपेक्षित नहीं करना चाहिए। मेरे अध्ययन के दायरे में ऎसी रचना भी आई है जिसमें केन्द्रीय चिन्ता भले ही स्त्री-देह के स्व-राज की लगती हो लेकिन एक पुरुष से प्रतिशोध के लिए दूसरे अधिक सशक्त पुरुष को पहले पुरुष से पीड़ित स्त्री के द्वारा सेक्स-मुक्ति के नाम पर आनन्द (संजीवनी) देकर अपने पक्ष में करना और प्रतिशोध लेना भले ही युद्ध और प्रेम में सब जायज है जैसी स्थापना के अनुकूल हो लेकिन सर्वथा ग्राह्य नहीं है भले ही अनुभव के स्तर पर (अपवाद की तरह) यह सच्ची घटना से प्रेरित प्रसंग ही क्यों न हो। सोचना होगा कि इसे देह की स्वतंत्रता कहें या देह का कपट अथवा देह की राजनीति या कुछ और। कभी -कभी इसी विमर्श के अन्तर्गत एक पत्नी का अपने पति से प्रतिशोध दूसरे पुरुष के प्रति संजीवनी के रूप में देह समर्पण के रूप में भी दिखाया जाता है। लेकिन याद रखना होगा कि सब एक जैसे नहीं होते जैसी धारणाओं के बावजूद दूसरे पुरुष के ’पुरुष’ न हो जाने की गारंटी नहीं होती । अत:पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्ति की राह ऎसी देह मुक्ति हो सकती है इस पर भी संदेह ही किया जा सकता है। वस्तुत: स्त्री विमर्श की राह प्रतिशोध से प्रतिरोध की ओर होनी चाहिए । तब स्वछंदता या स्वेच्छा भी स्वीकार्य होगी । अन्यथा पुरुष को पुरुष बनाए रखना ही कहलाएगा। मेरी निगाह में स्त्री विमर्श की एक बहुत ही सशक्त कृति चित्रा मुद्गल जी की आवां है । बकौल चित्रा जी, ‘विद्रोह, संघर्ष और कायरता, मनुष्य को ये सभी चीजें घर से वातावरण से ही मिलती हैं। मुझे भी घर के माहौल ने विद्रोही बनाया।’ संयोग देखिए कि इसी विद्रोह ने चित्रा जी को रचना संसार की राह भी दिखाई। पहली कहानी स्त्री-पुरुष संबंधों पर थी जो 1955 में प्रकाशित हुई। बहुचर्चित उपन्यास ‘आवां’ के लिए उन्हें व्यास सम्मान से नवाजा जा चुका है। चित्रा जी के, उनकी सोच को सामने लाने वाले स्त्री पात्र अपने अधिकार और स्वतंत्रता की लड़ाई में गजब की मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। उनकी एक कहानी ’लकड़बग्घा’ के माध्यम से भी इस तथ्य को बखूबी समझा जा सकता है ।
मातृसत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक समाज की यात्रा भी इसी पृथ्वी पर घटी है । पुरुष वर्चस्व न आसमान से टपका है और न ही जन्मजात है । जैसे स्त्री पॆदा नहीं होती, बनायी जाती है उसी प्रकार पुरुष भी पॆदा नहीं होता, बनाया जाता है। विडम्बना यह है कि इस बनाने में जाने-अनजाने पुरुष और नारी दोनों का हाथ होता है -कमोबेश । अत:मुझे तो वह सोच अधिक उपयुक्त लगती है जिसकी तहत पुरुषवर्चस्व और उसकी खामियों को पितृसत्तात्मकता में देखा जाता है । वोल्गा से गंगा को इस दृष्टि से भी पढ़ा जा सकता है । परम्परा के रूप में तुलसी का कलियुग वर्णन, महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां , मॆथिलीशरण गुप्त की साकेत वाली ऊर्मिला और यशोधरा, सुभद्रा कुमारी चॊहान की वीरांगना लक्ष्मीबाई का गुणगान, प्रेमचन्द के उपन्यास, जैनेन्द्र की कृतियां और कितनी ही अन्य पहले की कृतियों को पढ़ा और समझा जा सकता है । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने समय की किसी भी उत्तम सोच या उपलब्धि की पूर्व में तैयार हो चुकी एक पूर्वपीठिका हुआ करती है ।माना गया है कि नारीवाद की प्रेणता वर्जीनिया वुल्फ थीं जिनका लेखन काल 1915 से 1940 है । यह समय भारतीय नवजागरण का भी है और भारतीय नारी जागरण का भी । 1818 में राजा राममोहन राय ने सतीप्रथा विरोध किया था। 1829 में सतीप्रथा गैरकानूनी घोषित हुई । विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती आदि ने स्त्री शिक्षा पर ज़ोर दिया। 1857 में अमेरिका में पुरुष-नारी के समान वेतन को लेकरहड़ताल हुई थी। 1908 में ’वीमन्स फ्रीडम लीग’ की स्थापना हुई । 1911 में जापान में आन्दोलन हुआ । 1951 में संयुक्तराष्ट्र की महासभा में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का नियम पारित हुआ । 1905 में हिन्दी का पहला स्त्री काव्य संकलन “मृदुवाणी” मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा प्रकाशित किया गया जिसमें 35 कवियित्रियां संकलित की गईं । 1933 में “हिन्दी काव्य कोकिलाएं” और 1938 में “स्त्री कवि संग्रह” प्रकाशित हुए । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की “बालबोधिनी” पत्रिका अपना महत्त्व है । अगर पूर्व और पर के संदर्भ से अलग कर अपने स्वायत्त रूप में तुलसी की पंक्ति ’नारि मुई गृह संपति नासी, मूड मुड़ाइ होंहि सन्यासी ’ को पढ़ा जाए तो घरवाली नारि का अपार महत्त्व समझ में आ जाता है । यहां सन्यासी होने का महत्त्व नहीं पुरुष की दुर्गति के प्रति संकेत है । जिस संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है उसकी संकीर्णता का तो मैं भी पक्षधर नहीं हूं । गुप्त जी की यशोधरा सीधे-सीधे प्रश्न करती है -सिद्धि हेतु स्वामी गये, यह गॊरव की बात;/ पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याघात/ सखि, वे मुझसे कह कर जाते/ कह, तो क्या मुझको वे पग-बाधा ही पाते ? ध्यान दिया जाए कि पुरुष वर्चस्ववादी समाज में एक नारी अपने ’स्वामी’ को प्रश्नों के घेरे में ला रही है । हां ’पग बाधा’ वाली बात मेरी निगाह में भी पुरुषवादी मानसिकता का परिणाम है । यह पंक्ति नारी को पुरुष की समक्षता से थोड़ा नीचे ले आती है । जब सही अधिकार की बात हो तो ’बाधा’ के बारे में नहीं सोचा जाता ।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने समय की किसी भी उत्तम सोच या उपलब्धि की पूर्व में तैयार हो चुकी एक पूर्वपीठिका हुआ करती है ।माना गया है कि नारीवाद की प्रेणता वर्जीनिया वुल्फ थीं जिनका लेखन काल 1915 से 1940 है । यह समय भारतीय नवजागरण का भी है और भारतीय नारी जागरण का भी । 1818 में राजा राममोहन राय ने सतीप्रथा विरोध किया था। 1829 में सतीप्रथा गैरकानूनी घोषित हुई । विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती आदि ने स्त्री शिक्षा पर ज़ोर दिया। 1857 में अमेरिका में पुरुष-नारी के समान वेतन को लेकरहड़ताल हुई थी। 1908 में ’वीमन्स फ्रीडम लीग’ की स्थापना हुई । 1911 में जापान में आन्दोलन हुआ । 1951 में संयुक्तराष्ट्र की महासभा में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का नियम पारित हुआ । 1905 में हिन्दी का पहला स्त्री काव्य संकलन “मृदुवाणी” मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा प्रकाशित किया गया जिसमें 35 कवियित्रियां संकलित की गईं । 1933 में “हिन्दी काव्य कोकिलाएं” और 1938 में “स्त्री कवि संग्रह” प्रकाशित हुए । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की “बालबोधिनी” पत्रिका अपना महत्त्व है । अगर पूर्व और पर के संदर्भ से अलग कर अपने स्वायत्त रूप में तुलसी की पंक्ति ’नारि मुई गृह संपति नासी, मूड मुड़ाइ होंहि सन्यासी ’ को पढ़ा जाए तो घरवाली नारि का अपार महत्त्व समझ में आ जाता है । यहां सन्यासी होने का महत्त्व नहीं पुरुष की दुर्गति के प्रति संकेत है । जिस संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है उसकी संकीर्णता का तो मैं भी पक्षधर नहीं हूं । गुप्त जी की यशोधरा सीधे-सीधे प्रश्न करती है -सिद्धि हेतु स्वामी गये, यह गॊरव की बात;/ पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याघात/ सखि, वे मुझसे कह कर जाते/ कह, तो क्या मुझको वे पग-बाधा ही पाते ? ध्यान दिया जाए कि पुरुष वर्चस्ववादी समाज में एक नारी अपने ’स्वामी’ को प्रश्नों के घेरे में ला रही है । हां ’पग बाधा’ वाली बात मेरी निगाह में भी पुरुषवादी मानसिकता का परिणाम है । यह पंक्ति नारी को पुरुष की समक्षता से थोड़ा नीचे ले आती है । जब सही अधिकार की बात हो तो ’बाधा’ के बारे में नहीं सोचा जाता ।
महादेवी वर्मा का मत काफ़ी तर्क सम्मत लगाता है जब वे लिखती हैं :”पुरुष के द्वारा नारी चित्रण अधिक आदर्श बन सकता है , किन्तु यथार्थ के अधिक समीप नहीं । पुरुष के लिए नारीत्व अनुमान है नारी के लिए अनुभव।” मुख्य प्रश्न यह हो सकता है कि आखिर पुरुष में वे कॊनसे सुर्खाब के पर लगे हैं जिनके कारण स्त्री वही हो जैसा पुरुष चाहता ह । और यह चाहना भी सत्तात्मक या दम्भपूर्ण हो । अवधारणात्मक या इच्छाधर्मी तक नहीं । नारी-विमर्श यहीं से शुरु होता है । नारी के अपने होने यानी उसकी अस्मिता की पहचान और अर्जन के दायरे में उसकी तकलीफ़ें, उसके सपने, उसका चिन्तन, उसका विद्रोह, उसका अधिकार, उसके होने का स्वीकार, उसका आत्मविश्वास, अपने बूते पर खड़े होने की ताकत, उसके प्रतिरोध ही नहीं अपितु उसके प्रतिशोध, उसकी हार-जीत, और उसकी उपलब्धियां आदि सब आती हैं और साहित्य में नारी विमर्श यही है अथवा होना चाहिए । नारी-विमर्श पुरुष का नहीं बल्कि नारी की अस्मिता को रोंदने-कुचलने वाली पुरुष मानसिकता का विध्वंसक है या होना चाहिए । उसका सशक्तिकरण है । नारी-विमर्श अन्तत: ’नारी’’ को ’वहीं कटघरे में खड़े पुरुष’के स्थान पर स्थापित करना नहीं है अपितु ’कटघरे में खड़े पुरुष ’को नारी का उपयुक्त दर्शन कराना और मनवाना है । बेजगह कर दी गई नारी को उसकी पर लाना है । स्त्री-पुरुष को संबंधों के कुछ ही नहीं बल्कि तमाम रूपों और तमाम सामाजिक स्थ्तियों में रखकर स्त्री को बुनियादी तॊर पर उसकी जगह दिलाना है ।
आवां मेरे ऊपर आए चिन्तन की पुष्टि में खड़ा एक सशक्त गवाह है । या कहूं एक प्रेरक स्रोत है ।
सजग पाठक जानते होंगे कि आवां मात्र नारी विमर्श की ही कृति नहीं है बल्कि इसमें और बहुत से जरूरी संदर्भ भी आए हैं , जैसे श्रमिक-जीवन, श्रमिकों को लेकर ट्रेड यूनियन के बहुत से आयाम, क्रांति का आलाप जपते-जपते दलित, शोषितों, वंचितों का मसीहा बनने वालों का सच, दलित विमर्श, उलझे-सुलझे रिश्ते और उनकी कुत्सित तथा बिडम्बनापूर्ण यथास्थितियां, मनुष्यता की विभिन्न अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में खोज, अपने समय की राजनीतिक हलचलों जै से राजीव गांधी की हत्या आदि की झलक इत्यादि, लेकिन मेरी निगाह फिलहाल इस उपन्यास में आए नारी विमर्श पर टिकी है । यूं राजनीतिगत माहौल भी नारी विमर्श से अछूता नहीं है । एक दलित पात्र पवार जब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ब्राहम्ण लड़की नमिता से विवाह करके पूरी करने की बात करता है तो नमिता की प्रतिक्रिया का जायजा लीजिए -“जिस लड़की को चाहता है कोई, जिसे वह अपने जीवन-संगिनी के रूप में देख रहा, केवल वस्तु है उसके लिए? राजनीतिक महत्त्वाकांक्षियों के लिए संबंधों की गहनता खांचे-भर हैं चॊपड़ के? संकेत कर दूं कि यहां नारी विमर्श भी एक रेखीय नहीं है , अपितु वह अनेक कितने ही संदर्भॊं से गुथा-लिपटा है । अत: इस ओर सोचने पर और भी अधिक जिज्ञासा है । इससे पहले कि इस संदर्भ मैं , अपनी मूल बात पर आऊं, बता दूं कि इसमे एक पात्र स्मिता है जो एक शराबी, मटका किंग, पत्नी को पीटने वाला आततायी पति ही नहीं बल्कि अपनी ही पुत्री को देह मानकर व्यभिचार करने वाले पिता की बेटी है । ऐसे पिता से मुक्ति उसकी बाध्यता बन गई है । स्मिता एक संतुलित सोच की लड़की है लेकिन ’बाप आखिर बाप है ’ की चली आ रही सोच का अतिक्रमण उसके लिए जरूरी हो गया है । वह उपन्यास की प्रमुख पात्र नमिता को कहने पर विवश है कि ’शराब से हम लड़ सकते हैं , शैतान से नहीं। तुम से क्या छिपाऊं, ताई (बड़ी बहन) राक्षस के साथ अकेली घर में रहने से डरती है ।’ यह बेटी अपने क्रुर पिता को का नेस्तनामूद करने पर उतारू है । उसे अपने ननिहाल वालों से भी शिकायत है जिन्होंने ऐसे क्रूर और राक्षस पिता से अपनी बेटी( स्मिता की मां) का ब्याह किया। यह अलग बात है कि उसके मटका किंग पिता की हत्या किसी अन्य ने कर दी और नमिता के शब्दों में वह पितृहत्या से बच गई। वस्तुत: यह पिता-पुत्री के रिश्ते में से क्रूर पुरुष पिता के प्रति सजग बेटी (स्त्री) की सोच के माध्यम से सटीक नारी विमर्श है । इसके साथ ही, आत्मालोचन की सी शैली वाला यह विचार भी जोड़ दूं -“उसे (स्मिता की बहन) बरबाद होने देने में स्वयं उनकी (मां की) भूमिका कम नहीं। उस क्षण उन्हें (पिता को) दुष्कृत्य का प्रतिकार करना चाहिए था, मगर वे पति की प्रतिष्ठा पर आंच न आने देने के लिए सावित्री बन उनके अक्षम्य दुर्गुणों पर डाले रहीं।” लेकिन जै सा पहले भी संकेत दिया जा चुका है , यह उपन्यास एकांतिक सोच का कायल नहीं है । यहीं नमिता भी है जो अपने पिता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है । यह जानकर और वह भी खुद अपने पिता के मुख से कि किसी अन्य औरत से उसके पिता की एक संतान है जो उसकी सगी बहन है , उसकी प्रतिक्रिया है -“सुनंदा के पिता होकर बाबूजी क्या उसके बाबूजी नहीं रहे? चेहरे-मोहरे में तो कोई अंतर नहीं आया फिर…”। यहां पाठक चौकेगा जरूर। अर्थ की अनेक पर्तों से जूझने को विवश भी होगा। एक ओर सोचेगा कि पिता और सुनंदा की मां के बीच आपसी स्वीकृति रही होगी, इसलिए वह अपनी मां की दृष्टि से अनॆतिक हो सकता है लेकिन स्वाभाविकता की दृष्टि से इतना बड़ा अपराध नहीं। इत्यादि। यहां यह बताना भी जरूरी है कि स्मिता जैसी सचेत नारियां पुरुषवादी क्रूरताओं और धारणाओं की विरोधी हैं अन्यथा पुरुष उनकी जिन्दगी का आनन्ददायी प्राणी भी है । स्मिता की मित्रता पहले शरत से थी जिसे उसे उसकी अपनी तरह की मूर्खता के कारण छोड़ना पड़ा। लेकिन वह रोने-पीटने, सकुचाई-लज्जित भावुक नारी नही है । वह नया दोस्त विक्रम खोज लेती है । नमिता और उसके बीच बहुत ही दिलचस्प संवाद होता है जिससे स्मिता के माध्यम से अपने होने या स्व के प्रति स्वतंत्र और सचेत नारी का विमर्श सामने आता है —
“(नमिता) शरत से मित्रता खत्म?”
“(स्मिता) खत्म ही समझ। बेवकूफ है साआssला जाहिल…”
:”विक्रम आज का सच है ।”
इसके बाद जब नमिता शरत को छोड़ने का कारण विस्तार से जानना चाहती है तो वह शरत और अपने बीच हुई बातचीत का किस्सा बताती है जो तब हुई जब स्मिता के यह कहने पर,” शरत!बड़ी जोर से तुम्हें प्यार करने का जी हो रहा है । चलो, कहीं किसी होटल में एक सस्ता-सा कमरा लेकर मिलते हैं ..”, शरत अपने एक दोस्त भानु के कमरे में अकेले मिलने की बात करता है । अब बातचीत जानिए जिसमें पहला संवाद स्मिता (नारी लेकिन आज की सचेत नारी का है )–
“….और सुनो एक काम करो।”
“बोलो।” उमगते हुए शरत ने पूछा।
“कंडोम का पैकट साथ में लाना न भूलना।”
“(नमिता से) ’शरत मेरी बात सुनकर सकपकाया।’
“कहां मिलएगा कंडोम?”
“दवाओं की दुकान पर!”
“लेकिन..”
: अब कॊन-सी दुविधा हो गई?”
“उसे इस्तेमाल कॆसे करते हैं , मुझे मालूम नहीं।”
“कंडोम इस्तेमाल करना नहीं आता! जो कुछ और करना होता है उसे भी जानते हो या नहीं?” चिढ़ छूटी उस पर।
“बहुत अच्छी तरह! कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें।” सफाई दी पट्ठे ने।
” (नमिता से) ’मेरा तो पारा आपे से बाहर हो उठा।’
” मैंने कहा, मुझे होगी। इसलिए होगी गधे की औलाद कि मैं तेरे बच्चे की कुंवारी मां नहीं बनना चाहती और जो लड़का कंडोम इस्तेमाल करना नहीं जानता, वह मेरा प्रेमी होने के काबिल नहीं। बॆठ घर में।” गुस्से से फोन पटक दिया मैंने ।
“हर दूसरे-तीसरे रोज पगलाया-सा फोन खटखटता रहता है । मेरी ’हेलोs सुनते ही रंडीरोना शुरु। फोन पकड़े मैं निशब्द उसकी गिड़गिड़ाहट सुनती रहती हूं। कुछ देर बाद फोन रख देती हूं। वॆसे तो हरामखोर मर्द रोते नहीं…साआल्ले, रुलाने पर ही रोते हैं, रुलाने वाला चाहिए।”
निश्चित रूप से ऊपर का किस्सा बहुतों को अटपटा लगेगा और नमिता के सुर में सुर मिला कर कहेंगे कि यह प्रेम समझ के बाहर है , लेकिन इसके गहरे में जाकर चिन्तन किया जाए तो अन्तत: नारी सशक्तिकरण की गंध ही पाएंगे। नमिता भी अपने आपको श्रमिकों का बहुत बड़ा हितैषी समझने वाले क्रांतिकारी और अपने पिता के मित्र अन्ना की दी गई बहुत जरूरी नॊकरी को ठुकराती है क्योंकि “कभी-कभी नॊकरी से भी ज्यादा जरूरत होती है अपने सम्मान की रक्षा।” उपन्यास में उम्र में कहीं ज्यादा अन्ना की नमिता के प्रति अकेले केबिन में जो हरकत दिखाई गई है वह विचित्र है – अश्लील है लेकिन बलात्कार नहीं लगती।अनूठी। विस्तार से फिर कभी।
वैसे पुरूषवादी सोच के चलते औरत के मातृत्व की अनिवार्यता, अर्थी को औरत के द्वारा कंधा देने अथवा क्रियाक्रम करने पर सवाल आदि के मध्यम से भी नारी-चेतना के मसले बखूबी सामने आए हैं। चोट उस नारी विरोधी सोच पर भी की गई है जिसके चलते नारी की आत्मनिर्भरता की भी गलत संदर्भॊं में, पुरुष के वर्चस्व के हित में व्याख्या करने की कोशिश की जाती रही है –” यह सरासर लड़कियों का अपमान है कि वे इसलिए आत्मनिर्भर बनें कि उन्हें एक अदद अच्छा घर-वर मिले। आत्मनिर्भर लड़की को घर-बार साधारण भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है ? न भी ब्याह करे तो कॊनसी आफत? नॊकरी करे, खुश रहे।” गॊर इस कथन पर भी किया जाए -” आत्मनिर्भर होने की परिभाषा है , स्वयं के बुद्धि-विवेक का उपयोग, न कि पुरुषों के समक्ष आर्थिक सक्षमता।” साफ है कि यहां जोर उचित मानसिक बदलाव पर है , निरी भॊतिक सम्पन्नता पर नहीं। और गॊर जरा इस कठिन प्रश्न भी करते चलें जो चली आ रही सोच को हतप्रभ और क्षुब्ध कर सकता है लेकिन सही दिशा में सोचने पर विवश करता है -“जननी होना उसे गुलाम बनाए रखने की शर्त हो तो मजबूरी से स्वयं को मुक्त कर लेना उसकी अनिवार्यता नहीं? क्यों झेले वह सब जो उसे मनुष्य की श्रेणी से अपदस्थ करता हो?” पति-पत्नी के बीच देह संबंध स्वाभाविक और मान्य हैं लेकिन यदि संबंध बलात्कार की श्रेणी में आ जाए तब? तब चित्रा जी नमिता के कार्यालय की साथी गौतमी से कहलवाती हैं -“पति क्या होता है, आधिकारिक बलात्कारी! अथोराएज्ड…मैंने अशोक को उस अधिकार से वंचित रखा है कि जब मन किया, बीबी सो रही हो, जग रही हो, काम में व्यस्त हो, मरजी हो, न हो–उठाकर बिस्तर पर पटक लिया…।” जरा गॊतमी की फिलोसफी पर गॊर कर लिया जाए जो बहुत हद तक नारी-चेतना की पक्षधर भी हे और तर्क सम्मत तथा व्यवाहारिक भी- “देह को लेकर अंतर्व्याप्त रूढ़ि से मुक्त होने का सब से कारगर उपाय है , उसे चर्चा का विषय बना लो। तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत यॊनाकांक्षी स्त्री हूं। वास्तव में मैं ऎसी नहीं हूं। यॊन मेरे लिए उन्माद का विषय नहीं। इच्छा हो आए, बात अलग, वरना बगल में लेटे हुए हृष्ट-पुष्ट पति को अशोक को धरती-हिलाऊ हस्त-मॆथुन करना पड़ता? उतने मतलब के लिए एखुआ ही जा सकता है ।” उपन्यास में स्त्री के विवाह की जरूरत पर भी कुछ न कुछ विचार किया गया है । माना गया है कि विवाह हो जाए तो ठीक लेकिन न हो पाए तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाती। नमिता का पवार की मां से कहा गया यह वाक्य देखिए-“पांव पर खड़ी हूं अपने। खड़ी रहने को दृढ़ हूं। मुनिया और छुन्नु को आत्मनिर्भर बनाना है । ब्याह का क्या है , हो जाएगा। नहीं हो पाया तो मुझे नहीं लगता कि बिना ब्याह के मेरी सारी दुनिया उजड़ जाएगी।”एक अन्य सशक्त पात्र सुनन्दा तो और भी आगे बढ़कर कहती है -” मेरा मातृत्व ब्याह के टुच्चे प्रमाणपत्र का मोहताज नहीं।” नारी में, मनुष्योचित अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहते हुए अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता से लॆश होना एक सही नारी विमर्श है , यह बात इस उपन्यास में बखूबी रेखांकित हुई है । अकेले और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर। पुरुष या पुरुषों के साथ-साथ। आगे या पीछे नहीं।सोच की खूबसूरती यह है । एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसी बात को यूं समझा जा सकता है – “बाध्यता (स्वेच्छा के विरुद्ध करने) से व्यक्ति का उन्मेष कुंठित होता है । स्वाभाविक प्रकिया है । प्रत्येक युवा हृदय के कुछ सपने होते हैं । एक आवां होता है आंच से दहकता जिसकी पकावट से वह आकांक्षा की भीति उठाता है । छाजन छाता है ।” उपन्यास की प्रमुख पात्र नमिता को काम मिला था नारियों को जागरूक करने का। जिस उत्साह, प्रतिबद्धता से वह स्त्रियों को जागरूक करने, पीड़ित स्त्री के हक में उसके पास पहुंचने के लिए चाली नुमा झोंपड़ियों में जाती है यह भी अपने ढंग से नारी-विमर्श अर्थात नारी सशक्तिकरण का ही एक रूप है ।
वस्तु ही नहीं भाषा-लहजे आदि के स्तर पर भी, पुरुष वर्चस्विता पर हावी होते नारी चेतना के स्वर भी यहां बिखरे मिलेंगे। एक-दो उदाहरणों से बात को समझना आसान होगा। इस दृष्टि से कृष्णा सोबती और मृदला गर्ग आदि की भाषा को भी देख जा सकता है । खुद से ही शब्द उधार लेकर कहूं तो कृष्णा सोबती ने जब यारों के यार और मित्रो मरजानी जै सी कृतियां और ’मर्द रिझाऊ’ नहीं बल्कि ’मर्द मारू’ भाषा दी तो हंगामा होना स्वाभाविक था । पहली बार हिन्दी कहानी ने स्त्री के पारम्परिक ढके-दबे, सुरक्षात्मक, सांकेतिक,अर्द्ध छवि देत वाले सांस्कारिक रूप की कॆद से निकल कर ’बोल्ड’ होते हुए देखा था- “मित्रो अपने दोनों हाथों से अपनी छातियां पकड़कर पूछती है ,सच कहना जिठानी सुहागवंती, क्या ऎसी छातियां किसी और की भी हैं ?” ध्यान देना होगा कि यहां रचनाकार स्त्री है और पात्र भी स्त्री है । इसे चटखारे लेने वाले देह विमर्श के खाते में डाल कर नहीं समझा जा सकता । स्त्री की भी अपनी देह-दुनिया है । वह केवल पुरुषार्थ देह नहीं है । उसकी देह केवल पुरुष को समर्पित करने की वस्तु नहीं है , अपने से उपभोग करने के लिए भी है । सहवास का सही अर्थ भी शायद यही है । स्वाभाविक है कि विमर्श पर उतर कर स्त्री द्वारा रचे गए साहित्य की भाषा भी उसमें उभरे तीखे प्रश्नों की भांति तीखी यानी पुरुष वर्चस्ववादियों के लिए तीखी और बेशर्म ही होगी। अत: पुरुषवर्चस्ववादियों की हिप्पोक्रेसी पर भी समकालीन केन्द्रीय स्त्री-लेखन बज्रपात ही करता है । चित्रा मुद्गल की विमला बेन, जो स्त्री की नृशंस हत्या करने वाली पुरुष मानसिकता पर ही प्रश्न नहीं उठाती अपितु हत्या की शिकार हुई नारी-विमर्श के बड़े आयाम को मजबूती से सामने वाली एक प्रमुख पात्र सुनन्दा की अर्थी को कंधा देने की पहल करने वाली हठी महिला है , पुरुषों को अंगूठा दिखाती हुई इस धाकड़ भाषा में नमिता से बात कर सकती है -” अक्सर संडास का उपयोग करने वाले पुरुष संडास की कुंडी नहीं चढ़ाते और किसी महिला के ’धाड़’ से दरवाजा खोलते ही लघुशंका के लिए खड़े चॊंककर पलट पड़ते…सोचो, क्या दिव्य नजारा होता होगा!” विमला बेन की कभी अति सुंदर रही, भारी-भरकम देह हंसी से बेकाबू हुई। एक दूसरे प्रसंग में नमिता की मां का यह कथन भी पढ़िए -“अरी छिनारियो! (यहां हिन्दी जगत में घटे एक छिनाल प्रसंग को भी याद कर लीजिए)। सब गोलबंद रहोगी तो मजाल, जो किसी रोआं उखड़ जाए। चिल्लरों सी खनखनाओगी तो बूढ़ा तुम्हारी झां..न उखाड़ ले तो नाम बदल देना मेरा।” इसे चित्रा जी की लेखकीय अदा ही कहा जाएगा कि वे तुरन्त नमिता को सामने लाकर उपर्युक्त कथन को संतुलित कर देती हैं – ” उफ! सहमकर उसने (नमिता ने) कानों पर हाथ रख लिया। क्या हो गया यह मां को? मां के मुंह से भदेस गालियां निकलना कोई अनहोनी बात नहीं। मगर बेटी के सामने लगाम-लिहाज छोड़ने पर विस्मय अवश्य हुआ उसे।” इस प्रकार की भाषा और लहजे के द्वारा उस रूढ़िगत सोच पर भी आघात किया गया है जिसके द्वारा बोल्ड होना अच्छी लड़की का गुण नहीं माना जाता। यहां यह बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा और कि चित्रा जी ने बहुत से स्थानीय(प्रादेशिक) शब्दों और मुवाहरों की ताकत से भी इस उपन्यास को समृद्ध किया है । उपन्यास की प्रमुख पात्र नमिता को काम मिला था नारियों को जागरूक करने का। जिस उत्साह, प्रतिब्द्धता से वह स्त्रियों को जागरूक करने, पीड़ित स्त्री के हक में उसके पास पहुंचने के लिए चाली नुमा झोंपड़ियों में जाती है यह भी अपने ढंग से नारी-विमर्श अर्थात नारी सशक्तिकरण का ही एक रूप है । वस्तुत: उपन्यास के महिला पात्र (नमिता, नमिता की माँ, स्मिता, हर्षा, गॊतमी, मेम साहिब, विमला बेन, सुनन्दा, सुनन्दा की मां किशोरी बाई आदि) प्राय: अपनी-अपनी शक्ति और सीमा के साथ उपस्थित हुए हैं । यह बात अलग है कि चित्रा जी की नारी-चेतना संबम्धी दृष्टि सबके बीच पिरोयी हुई महसूस होती रहती है । उपन्यास का अंत केन्द्रीय पात्र नमिता अपनी सगी बहन सुनन्दा की मां किशोरी बाई की खोली में जाने पर ही होता है । यह अंत होकर भी अंत नहीं लगता और पाठक को बहुत कुछ प्रश्नों के घेरे में डाल कर मानता है ।याद रहे कि सुनन्दा की मृत्यु (हत्या) के बाद किशोरी बाई ने नमिता के बीमार पड़े पिता को चिट्ठी लिखी थी -“पांडे बाबू! आपकी सुनन्दा (कुंवारी माँ) नहीं रही। उसे हमने नहीं मारा। अपनी मॊत का कुआं जिद्दन नेण खुद ही खोद लिया। मैं क्या करती? उसे किस विधि बचाती?” नारी -विमर्श की दृष्टि से किशोरी बाई के व्यक्तित्व पर गॊर किए जाने की जरूरत नहीं है क्या? और इसके बाद ही पिता ने नमिता को बताया था-“नमी सुनन्दा तुम्हारी सगी बहन थी।” बताता चलूं कि नमिता भी अपने देह संबंध विवाहित-धनी संजय नामक शख्स से बनाती है ,जिसकी पत्नी उसे संतान देने में असमर्थ है , और प्रारम्भ में कुंवारी मां नहीं बनना चाहती हालांकि बन जाती है । हादसे वश बच्ची मर जाती है और संजय की आशा भी मर जाती है ।
अब मैं ऊपर संकेत देकर छोड़ दी गई मूल बात पर आता हूं जो असल में इस उपन्यास की एक बड़ी उपलब्धि है । उपन्यास में एक नारी पात्र सुनन्दा है जो मेरी निगाह में इस उपन्यास की नारी चेतना से सम्पन्न सबसे सशक्त स्त्री पात्र है । साथ ही चित्रा जी की सृजनात्मक उपलब्धि भी।
सुनन्दा विवाह के लिए अपने प्रेमी ’सुहै ल’ के धर्म परिवर्तन के आग्रह या शर्त को मानने से इंकार कर देती है क्योंकि उसे सहज रूप में लगता है कि वॆसा करने से उसकी अपनी पहचान या अस्मिता दाव पर लगी लगती है । शर्त या आग्रह के नाम पर उसे अपना नाम तक बदलना अपने होने के विरुद्ध लगता है । बुनियादी तॊर पर यह मसला दो प्रेमियों तक सीमित न रह कर बहुत दूर तक जाता है । अत: यहँ विरोध ’सुहै ल’ का नहीं है । एक अनुचित और अग्राह्य अवधारणा या व्यवस्था का है । इसीलिए यहाँ विशिष्ट सामान्य या असाधारण साधारण बन जाता है । विशिष्ट अनुभव सबका हो जाता है । अत:सुनन्दा का बिना ब्याह के न केवल देह संबंध बनाना बल्कि ’प्राउड’माँ भी बन जाना देह मुक्ति के एक नए व्याकरण को सामने लाता है और अपने को मनवाता भी है । साथ ही ’कुँवारी माँ’ वाली चली आ रही स्त्री विरोधी धारणा पर लेखिका कुठाराघात भी करती है। भले ही मठाधीसों को यह हरकत रास न आए। ऎसी राह पर चलने वाली जागरूक नारियों के सामाने चुनॊतियां भी बहुत होती हैं और प्राणॊं तक के खतरे भी। नारयण सुर्वे, इसी उपन्यास में स्त्री चेतना की पक्षधर सुनन्दा को अपनी हवस से इलाके के अमन-चॆन को आग लगाने वाली कहता है । एक जगह रूपक के बहाने उसे कुतिया भी कहा गया है । देखिए-” सड़क पर जब कोई कुतिया आवारा घूमती नजर आती है , कामोत्तेजित कुत्ते एक साथ उसकी दुम उठा…..।इस क्रांतिकारी सुनन्दा के होश बहुत जल्दी ठिकाने आ जाएंगे।” और अन्तत: सुनन्दा की रात में हत्या कर दी जाती है । लेकिन सुनन्दा की दृष्टि या दिशाबोध की हत्या करने की किसमें ताकत है ? वस्तुत: यह प्रसंग बहुआयामी है । एक ओर दो अलग-अलग धर्मों से होने के कारण विवाह न कर पाने की वजह है तो दूसरी ओर इसी वजह के साम्प्रदायिक उन्माद बनने का खतरा है । गर्भ गिराने न गिराने का मसला भी है । एक अन्य आयाम कुंवारी माँ वाला है जो सामाजिक मान्यता से तो जूझने वाला है ही संवॆधानिक रूप में भी अड़चन करता है । पहले इस अन्य आयाम को लें। सुनन्दा जो मे ऎण्ड बेकर में काम करती है , चाहती है कि उसकी बच्ची को क्रेच की सुविधा मिले। वे सारी सुविधाएं मिलें जो कम्पनी अन्य माँ कर्मचारियों को देती है । इस पर कम्पनी का तर्क है कि”आप कुंवारी हैं । जचकी की सुविधाओं की कानूनन अधिकारिणी नहीं।” उसके साथ हो रही इसी ज्यादती के विरोध में नमिता सुनन्दा से मिलने के लिए पहली बार उसके घर जाती है और उन दोनों के बीच जो संवाद होता है वह सहज ही नारी-विमर्श के एक सशक्त पक्ष को उतनी ही मजबूती से सामने ले आता है । कम्पनी के द्वारा कुंवारी माँ की जचकी से सम्बद्ध तर्क पर सुनन्दा का भारी मारक तर्क देखिए-” देखिए दीदी, सुविधा का प्रावधान गर्भवती स्त्री और उसके बच्चे को लेकर है , न कि कुंवारी माँ या ब्याहता माँ के विशेषण के लिए। कुंवारी माँ क्या ब्याहता माँ के ही समान जचकी के घोर कष्टों से होकर नहीं गुजरती?–माँ बनना किसी के निजी मामले की बजाय कम्पनी का मामला कॆसे हो गया?” प्रश्न यहीं तक सीमित नहीं रहता क्योंकि इसका दूसरा संदर्भ भी है और वह और भी बड़ा है । यह ठीक है कि कुंवारी माँ की जचकी को लेकर कम्पनी वालों के अन्याया के प्रति जागरूकता(प्रतिरोध) जरूरी है और इसके लिए ही ट्रेड यूनियन के दफ्तर से विमला बेन ने नमिता को भेजा गया था। लेकिन सुनन्दा तो इससे भी बड़े एक और खतरे से भी जूझ रही थी और वह था साम्प्रदायिक उन्माद का क्योंकि उसकी कोख का बच्चा एक अन्य (मुस्लिम) धर्म के पुरुष की देन था। हम सब जानते हैं कि विशेष रूप से हिन्दूओं और मुस्लमानों में बहुत से ऐसे कट्टरपंथी हैं जो अपनी रोटियां सेंकने के लिए साम्प्रदायिक उन्माद और दंगे करती रहने की फिराक में रहते हैं , और इसके लिए छोटे-छोटे बहानों को भी भुना लिया करते हैं । सुनन्दा के ही मुख की बात जानिए-“धर्माधों के लिए मैं एक बहाना भर हूं। मैं बहाना न रहूं तो कल वे कोई और बहाना तलाश लेंगे। गढ़ लेंगे।गढकर उसमें तेल के पीपे उलींचेंगे। दीदी जरूरत है , उसकी कलाइयां धर लेने की –मजबूती से, ताकि वे हाथ न छुड़ा पाएं। तीली न सुलगा पाएं। और य काम कोई और नहीं , सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं ।” इस संवाद में बहाने गढ़ने और केवल स्त्रियां कर सकती हैं पर ध्यान जाना चाहिए। अर्थात किसी समस्या के समाधान को विकल्पहीनाता के चॊराहे पर नहीं खड़ा किया जा सकता। आगे और भी स्पष्ट ढ़ंग से सुनन्दा कहती है – “उनसे (बिमला बेन से) कहिएगा दीदी! कुंवारी माँ की जचकी का हक लड़ने से पहले वे साम्प्रदायिक उन्माद को खत्म करने की लड़ाई लड़े, वरना सब बरबाद हो जाएगा। खोली-खोली में घुसकर हिन्दू-मुसलमान औरतों को इतना जागरूक कर दें कि वे अपने घरों के उन्मादी मर्दों के हाथों से उनकी कटारें छीन लें।” यही नहीं सुनन्दा किसी भी जागरूक मनुष्य की तरह धार्मिक उन्माद को असामाजिक कृत्य मानते हुए उसके पूरी तरह खिलाफ है और इसीलिए वह इस समस्या से दो-दो हाथ करने के लिए, दबाव की रणनीति की तहत, सुझाव देती है कि मुस्लिम और हिन्दू स्थ्रियों को अपने मर्दों को धमकाना चाहिए कि यदि उन्होंने असामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया तो वे बाल-बच्चों समेत आत्मदाह करेंगी। अगर नमिता को सुनन्दा की अंतश्चेतना अत्यंत प्रखर लगी है तो क्या गलत है ? चित्रा जी इतने पर भी नहीं रुकतीं। वे जमा जमा कर बताना चाहती हैं कि जाति-धर्म का बवाल माचाने वाले बुनियादी तॊर पर पुरुष होते हैं । स्त्रियां को अवसर मिले तो वे इस बवाल को शांत करने वाली होती हैं । मर्दों की जो फितरत प्राय: अनुभव के दायरे में आती है, वह है घर में अपनी औरतों की तो फिर इज्जत कर ली लेकिन सड़क पर निकलेते ही औरतों के प्रति कुत्ते हो लिए। नमिता ने सुनन्दा की स्त्री संबंधी सोच और ताकत को समझ लिया है इसीलिए एक स्थान पर वह बताती है -“सुनन्दा का कहना है कि तनाव के इस माहॊल में औरत के सहयोग और उसकी निर्णायक भूमिका के विषय में विचार किया जाना जरूरी है । स्त्री चेतना कम से कम पुरुषों की बनिस्बत जाति-धर्म की बंधक नहीं बल्कि वे सर्वोपरिता की टकराहट से बाहर हैं।”
किस्सा यह है कि हिन्दू धर्म की सुनन्दा और इस्लाम धर्म के सुहै ल के बीच प्रेम हो जाता है और वे दोनों विवाह करना चाहते हैं। सुनन्दा प्रेम के चलते गर्भवती भी हो जाती है । विवाह के बीच धर्म या सम्प्रदाय आड़े आ जाता है । ससुराल वाले इस्लाम कबूल करने की शर्त रखते हैं जो गर्भवती होने के बावजूद स्वचेता सुनन्दा को एकदम मंजूर नहीं। वह तो अपना नाम बदलने को भी तैयार नहीं। विवाह होने की संभावना न रहने पर भी वह अपने गर्भ को गिरानेवाली सोच भी नहीं रखती। यदि हम उसके इंकार का कोई एक कारण खोजना चाहें तो पता चलएगा कि वह है उसकी अपने होने को स्वीकृति देने की चेतना, अपने निर्णय खुद लेने के अधिकार के प्रति जागरूकता। वह दो व्यक्तियों के बीच के ब्याह को लेकर मनुष्य को बांटने और उसके नाम पर एक दूसरे को नेस्तनाबूद करनेवाली मानसिकता और सोच की कट्टर विरोधी है । उसका तर्क इतना भर नहीं है कि वह शर्त के नाम पर अन्य धर्म अथवा अन्य धर्म का नाम नहीं रखना चाहती बल्कि वह तो दूसरे पक्ष को भी ऎसा करने को बाध्य नहीं करना चाहती। ब्याह के बाद भी हिन्दू हिन्दू रहे और मुसलमान मुसलमान तो क्या हर्ज है । हां कॊई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो बात अलग है । वस्तुत: सुनन्दा ने सुहै ल से ब्याह करने से कभी ईंकार नहीं किया। वह बस हिन्दू-मुस्लिम एकता को धर्म से ऊपर देखना चाहती थी। वह हिन्दू होकर मुसलमान से विवाह करना चाहती थी। वह आडम्बरों से ऊपर रहने वाली स्त्री है । वह तो कोर्ट मैरिज करने तक को तैयार थी। सुनन्दा के शब्दों में कहें तो, ” प्रश्न यह था दीदी कि मैं औरों की सुख-सृष्ट के लिए अपने सच को घोंट दूं या अपने ’स्व’ के संरक्षण के लिए उसके उगने को देह धरने दूं, उसे एक पूरी की पूरी काया ग्रहण करने दूं….सुहै ल ने प्रेम करने के समय तो कोई शर्त नहीं रखी? ब्याह करना होगा तो उससे नहीं इस्लाम से करना होगा….या उसे हिन्दुत्व से?” “जो शर्त पहले शर्त नहीं थी, बाद में शर्त क्यों बने? समझॊते को मैं भी राजी नहीं हुई। मुझे लगा दीदी, समझॊते ’आदि’ तो होते हैं अंत नहीं।”
गौर से देखा जाए तो यहां स्त्री-पुरुष ही नहीं बल्कि दो व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के चले आ रहे तथाकथित अधिकारों और अधिकारहीनताओं की ऎसी विवेचना उपलब्ध हुई है जो अधिकारों की बलपूर्वक छीना झपटी से ऊपर उठकर समझ के साथ एक -दूसरे को मनुष्य समझते हुए, समान और जायज अधिकार देने की दिशा में अग्रसित करती है । दोनों को ही स्पेस या जगह देने का पक्ष सामने लाती है । स्वेच्छा के रूप मे देह मुक्ति और स्त्री विमर्श की एक बहुत ही सशक्त कृति है आवां ।
#डॉ. दिविक रमेश
परिचय: डॉ. दिविक रमेश सुप्रतिष्ठित वरिष्ठ कवि,बाल-साहित्यकार,अनुवादक एवं चिन्तक के रूप में जाने जाते हैंl २०वीं शताब्दी के आठवें दशक में अपने पहले ही कविता-संग्रह ‘रास्ते के बीच’ से चर्चित हो जाने वाले आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि हैं। ३८ वर्ष की आयु में ही ‘रास्ते के बीच’ और ‘खुली आंखों में आकाश’ जैसी अपनी मौलिक साहित्यिक कृतियों पर सोवियत लैंड नेहरू जैसा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले इस पहले कवि ने १७-१८ वर्षों तक दूरदर्शन के विविध कार्यक्रमों का संचालन किया है। भारत सरकार की ओर से दक्षिण कोरिया में अतिथि आचार्य के रूप में आपने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दिविक रमेश का जन्म १९४६ में दिल्ली के गांव किराड़ी में हुआ और १९८६ से उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे प्रमुख शहर नोएडा में स्थाई रूप से रह रहे हैं। इनका वास्तविक नाम रमेशचंद शर्मा हैl आपकी अनेक कविताओं पर कलाकारों ने चित्र और कोलाज़ आदि बनाए हैं,जिनकी प्रदर्शनियां भी हुई हैं। इनकी बाल-कविताओं को संगीतबद्ध किया गया है। जहां इनका काव्य-नाटक ‘खण्ड-खण्ड अग्नि’ बंगलौर विश्वविद्यालय की एम.ए. कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित है,तो इनकी बाल-रचनाएं पंजाब, उत्तर प्रदेश,बिहार और महाराष्ट्र बोर्ड, कर्नाटक, केरल तथा दिल्ली सहित विभिन्न स्कूलों की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जा रही हैं। इनकी कविताओं-साहित्य पर पी-एच.डी. उपाधि के लिए शोध भी हो चुके हैं। आपके साहित्य पर शोधपरक-आलोचनात्मक कार्य होने के साथ ही समकालीन हिन्दी काव्य प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में रचनाओं का अध्ययन भी किया गया हैl इनकी कविताओं को देश-विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संग्रहों में स्थान मिला है। इनमें से कुछ अत्यंत उल्लेखनीय हैं-इंडिया पोयट्री टुडे (आई.सी.सी.आर.), न्यू लैटर (यू.एस.ए.) स्प्रिंग-समर और इंडियन लिटरेचर आदि हैंl आप अनेक देशों-जापान, कोरिया, बैंकाक, हांगकांग, सिंगापोर, इंग्लैंड, सहित स्पेन आदि की यात्राएं कर चुके हैं। २०११ में दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवामुक्त हुएl दिल्ली विश्वविद्यालय में १९७० से कार्यरत थे। वर्तमान में आप सदस्य-परीक्षा तुल्यता समिति, महात्मा गांधी हिन्दी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय(वर्धा) हैं। आपको प्रमुख पुरस्कार-सम्मान के रूप में दिल्ली हिन्दी अकादमी का साहित्यिक कृति पुरस्कार १९८३ में,सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार १९८४ में,गिरिजाकुमार माथुर स्मृति पुरस्कार १९९७,एनसीईआरटी का राष्ट्रीय बाल-साहित्य पुरस्कार(१९८८) सहित श्री गोपीराम गोयल सृजन कुंज पुरस्कार-२०१६(श्रीगंगानगर) के अलावा भी कई सम्मान प्राप्त हुए हैंl आपकी प्रकाशित कृतियों में कविताः‘रास्ते के बीच( १९७७ और २००३), ‘हल्दी-चावल और अन्य कविताएं’, ‘छोटा-सा हस्तक्षेप’,‘फूल तब भी खिला होता’,‘गेहूँ घर आया है`,वह भी आदमी तो होता है,बाँचो लिखी इबारत(२०१२),माँ गाँव में है,वहाँ पानी नहीं है,`से दल अइ ग्योल होन`(कोरियाई भाषा में अनुदित कविताएं) सहित ‘अष्टावक्र’(मराठी में अनुदित कविताएं) आदि हैंl आलोचना साहित्य में आपके नाम ‘कविता के बीच से’,‘नए कवियों के काव्य-शिल्प सिद्धांत’,‘साक्षात् त्रिलोचन’,‘संवाद भी विवाद भी’,समझा-परखा, और हिन्दी का बाल-साहित्य:कुछ पड़ाव(भारत सरकार)है। ऐसे ही आपके बाल साहित्य में कविता संग्रह:जोकर मुझे बना दो जी,हंसे जानवर हो हो हो,कबूतरों की रेल,छतरी से गपशप,अगर खेलता हाथी होली,तस्वीर और मुन्ना,एवं मधुर गीत भाग-३ और भाग-४ भी है। कहानी संग्रह की बात करें तो `धूर्त साधु और किसान`,सबसे बड़ा दानी,शेर की पीठ पर,बादलों के दरवाजे,घमंड की हार,ओह पापा के अलावा बोलती डिबिया तथा स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन आदि हैं। आपने लोक कथाएं: सच्चा दोस्त,पेड़ गूंगे हो गए और जादुई बांसुरी आदि रची हैं तो,आत्मीय संस्मरण:फूल भी और फल भी (लेखकों से संबद्ध) लू लू की सनक (कहानी संग्रह),बचपन की शरारत (सम्पूर्ण बाल-गद्य रचनाएं-२०१६),मेरे मन की बाल कहानियाँ आदि के अतिरिक्त बाल नाटक:‘बल्लू हाथी का बाल घर’,मुसीबत की हार आदि भी लिखी हैंl ‘खंड-खंड अग्नि’ की मराठी, गुजराती, कन्नड़ और अंग्रेजी अनुवाद सहित अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में रचनाएं अनुदित हो चुकी हैं। आपकी चुनी हुई बाल कविताओं का संग्रह : मैं हूं दोस्त तुम्हारी कविता का जल्दी ही प्रकाशन हो रहा हैl


