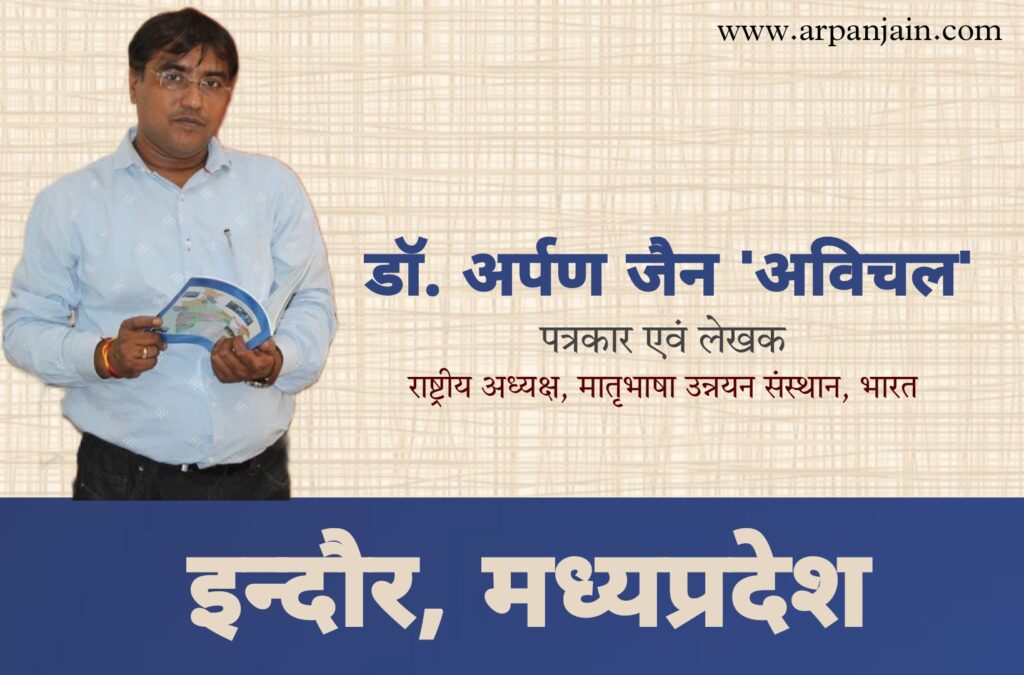
● डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
साहित्य उत्सवों का नाम बदलकर मौज मस्ती उत्सव कर देना ज़्यादा सार्थक और असरदार है क्योंकि इससे साहित्य के भीतर की मलीनता पनपने से बचेगी और साहित्य के नाम पर जनता से छलावा नहीं होगा।
जाड़े का मौसम आ चुका है और हर बार की तरह जाड़े की गुलाबी ठण्डक तमाम शादी-विवाह, अन्य आयोजनों के लिए अनुकूल भी है। इस समय देश का माहौल भी साहित्यिक हो रहा है, साहित्य उत्सवों की बाढ़–सी आई हुई है। कहीं साहित्य का जलसा है तो कहीं लेखक-लेखिकाओं की तफ़री के लिए पर्यटन उत्सव जैसा साहित्य महोत्सव। कहीं गाली-गलौच करने वाले वीडियो बनाकर प्रसिद्धि पाने वालों की साहित्य उत्सवों में आमद है तो कहीं झींगुर नृत्य वाली सेलेब्रिटी के शो हैं। बताओ भला कहीं से भी साहित्यिक न नज़र आने वाले ऐसे उत्सवों की बाढ़ में साहित्य कहाँ नज़र आ रहा है? या फिर साहित्य समाज का क्या भला हो रहा है, जो इस तरह के उत्सवों में बढ़–चढ़कर हिस्सेदारी ली जा रही है? विमर्श के नाम पर खोखली चुहल हावी है, निष्कर्ष के नाम पर सालों पुराने ढर्रे पर चलने वाला चलताऊ किस्म का बहाना। आख़िरकार साहित्य समाज भी बीते दिनों हुए टी ट्वेंटी विश्वकप के भारत-इंग्लैंड सेमी फ़ाइनल मैच में हार्दिक पण्ड्या की तरह हिट विकेट होने पर आमादा है। साहित्य कुनबे में जो स्वीकार्यता आ रही है, वह किसी भी तरह से गुणवत्ता की ओर इशारा भी नहीं कर रही है। वर्तमान दौर में देश में सालभर में लगभग 100 से अधिक बड़े और 500 से अधिक छोटे साहित्य उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इन उत्सवों में 5000 से अधिक लेखकों को बुलाया भी जाता है, दिन-प्रतिदिन यह आँकड़ा बढ़ भी रहा है। किंतु उत्सवों के फल की कहीं कोई चर्चा नहीं, शताधिक श्रोताओं का लश्कर, बीसियों किताबों का विमोचन, ‘मेरी तेरे साथ, तेरी मेरे साथ सेल्फ़ी’ की तर्ज़ पर उत्सवों, साहित्य मेलों में रचनाकारों की भीड़, अच्छा मीडिया कवरेज, दस-बीस ब्ल्यू टिक वालों की टिक-टिक, दर्जनभर खाने-पीने के स्टॉल, और रंगीन मिज़ाजों के लिए सुरापान के बीच गुज़रती शाम या कहें छलकती रात, यही सब हो रहा है आजकल साहित्य उत्सवों के नाम पर। फिर कहते हैं पाठक कहाँ है, क़िताबें बिकती नहीं, साहित्य पढ़ा नहीं जा रहा, समदर्शी नहीं है समाज, साहित्य का दायरा कुंद हो रहा है। तमाम बातों के बीच प्रश्न तो यह है कि ‘क्या साहित्य इस तरह से बच भी पा रहा है?’
साहित्य उत्सवों में टॉक शो, सेशन, बातचीत, चर्चा जैसे शब्द प्रायः चलन का हिस्सा है, बहुत हुआ तो आपबीती से निकलकर लोकबीती तक पहुँच जाएँगे, कहीं किताबों पर चर्चा के नाम पर लेखक और प्रकाशक की मार्केटिंग की जाएगी, कहीं कुछ शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाएगा, यहाँ तक कि उस शुल्क में इस बात का भी शुल्क होगा कि सेलेब्रिटी के साथ आप फ़ोटो खिंचवा पाएँगे, वक्ता तो खाने-पीने और रहने का इंतज़ाम पा लेगा पर बेचारा श्रोता न विचारों की क्षुधा शान्त कर पायेगा और न ही पेट की। अंततः उसे लौटना अपने ही मयार में होगा। शाम होते ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कहीं तो चुटकुलेबाजों का कवि सम्मेलन होगा या फिर कानफोड़ू रैप से सुसज्जित बैण्ड पार्टी। थोड़ी लाज बच जाए या आँखों का पानी ठहर जाए तो सुगम संगीत या किसी अच्छे कलाकार का संगीत कार्यक्रम हो पाएगा। सम्मान-पुरस्कार तो हलवा-पुरी की तरह बांटे जाएँगे। इसके बाद क्या, ढाक के तीन पात।
साहित्य उत्सवों का नाम बदलकर मौज मस्ती उत्सव कर देना ज़्यादा सार्थक और असरदार है क्योंकि इससे साहित्य के भीतर की मलीनता पनपने से बचेगी और साहित्य के नाम पर जनता से छलावा नहीं होगा। बच जाएगी साहित्य की अस्मिता अन्यथा आने वाले समय में साहित्य नाम से नफ़रत के सिवा कुछ शेष नहीं बचेगा। लोगों में उबाऊपन घर करने लगा है, लेखक समुदाय के पास लिखने से फ़ुर्सत नहीं है, न ही उन्हें किसी को पढ़ने की ज़रूरत है और न ही ख़ुद का लिखा कोई पढ़ रहा है या नहीं, यह सोचने का समय। लेखक तो बेचारा ऐसा निरीह प्राणी है जो यह सोचता है कि केवल उसी के लेखन से दुनिया बदल रही है, यदि उसने चिंतन नहीं किया तो यह धरती अपने अवसान को यानी प्रलय को प्राप्त कर लेगी। भले घर में बूढ़ी माँ पानी माँग-माँग कर थक जाए, बहू मोबाइल से बाहर नहीं निकलेगी पर फेसबुक पर वही बहू स्त्री विमर्श पर बीसियों आलेख लिख देगी, माँ और सास की महत्ता पर चालीस कविता लिख चुकी होगी और यह भी सिद्ध हो चुका होगा कि उसके समान न बहू है और जितना प्रेम उसके व उसकी सास के बीच है अन्यत्र दुर्लभ। भले चाहे जो कविताओं के साथ अपनी और सासू की फ़ोटो चिपकाई है वह भी महीनों या कहें सालों पुरानी हो, क्योंकि आजकल तो सास से बात करने की उस सो कोल्ड लेखिका बहू को फ़ुरसत नहीं है।
चिंतन इतना कि चरबा या कहें विचारों को कॉपी करके, शब्द बदलकर लिखने में भी हिचकिचाहट नहीं क्योंकि लिखने का उद्देश्य केवल सोशल मीडिया पर वाह-वाही पाना है, पचास-सौ लाइक पाने की जुगाड़ में लेखन भी मौलिक नहीं बचा, ऐसी स्थिति में साहित्य उत्सवों से निकलने वाले साहित्य अमृत का क्या होगा! वह तो मानो व्यर्थ ही बह जाएगा। जिस तरह देश में साहित्यकार मशरूम की तरह लगातार पैदा हो रहे हैं, उस हिसाब से तो साहित्य उत्सवों का बंटाधार तय है।
साहित्य उत्सवों के नाम पर जो साहित्य का कचरा किया जा रहा है और उस कचरे में जब साहित्य समाज ही शामिल हो रहा है तो पीड़ा होना लाज़मी है।
जबकि होना यह चाहिए कि साहित्य उत्सव में विशुद्ध साहित्यिकी विधाओं के उन्नयन, भाषा की चिन्ता और साहित्य गुणवत्ता पर विमर्श होना चाहिए, विमर्श किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए, जिससे वर्तमान और आगामी पीढ़ी तक भी साहित्य की उत्तरोत्तर उन्नति शामिल हो।
साहित्यकारों के सुखद भविष्य की चिंताओं का हल निकले, साहित्य के समदर्शी होने का समाधान निकले, साहित्य का असल चिंतन हो, चिंतन में सभी शामिल होकर एक जाजम पर आकर प्रगतिशीलता का स्थायी आधार निर्मित हो। वर्तमान समय में दिशाविहीन साहित्य जगत इन उत्सवों में केवल अपनी सुनाने के लिए नहीं बल्कि जग की सुनकर आनंददायक भविष्य के नवनिर्माण की परिकल्पना को साकार करें।
चिंता विहीन समाज चिन्तन से विमुख हो जाता है, जो कि आगामी पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु समाज के नैतिक मूल्यों के भी पतन का कारण बनता है। आज साहित्य समाज को नैतिकता की जड़ों की ओर पुनः लौटने की आवश्यकता है। समाज यदि चिन्तन–विहीन होने लग गया मतलब साफ़ तौर पर समाज रीढ़–विहीन होने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा क्योंकि समाज का मेरुदण्ड उस समाज का चिंतन, चिंतक और साहित्य है। इस दिशा में साहित्य उत्सवों के आयोजकों को भी सोचना होगा, तभी प्रगतिशील समाज का वैभव स्थापित होगा।
शब्द क्रान्ति का हवन करना चाहते हैं, साहित्य उत्सवधर्मिता के बीच जनमानस के ललाट का तिलक बनना चाहता है, किताबें राष्ट्रजागरण का अध्याय लिखना चाह रही हैं पर इन अस्तरीय उत्सवधर्मिता से साहित्य अपनी पैनी धार को कमज़ोर कर रहा है। कमज़ोर कन्धों पर भविष्य की बागडोर देखकर किताबें भी व्यथित हैं।
कवि राजकुमार कुम्भज के शब्दों में ‘क्या किताबों में ज़रा-सा भी नमक नहीं बचा’ सम्भवतः इसी कारण से अब किताबें उन्माद के उत्सवों के बीच घिर गई हैं और समाज को दिशा देने में ख़ुद को अकेला पा रही हैं। ऐसे दौर में सभासद की भाँति साहित्य के वरेण्य और अग्रजनों से लेकर तो सभी सुधीजनों को कमान संभालनी चाहिए, उत्सवधर्मिता के बीच गुणवत्ता के लिए लड़ना होगा। गुणवत्ता बरक़रार रहे, यह अभिजीत कार्य करना होगा। जिन विशुद्ध साहित्यिक आयोजनों में गुणवत्ता और साहित्य की महनीय गरिमा का ख़्याल न रखा जाए, वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। या तो वह आयोजन साहित्य उत्सव न हो तो फिर उसे साहित्य उत्सव का नाम देकर साहित्यजगत के साथ छलावा भी नहीं होना चाहिए। शब्द तब ही क्रान्तिनाद करेंगे, साहित्य तब ही ज़िन्दाबाद होगा।
डॉ. अर्पण जैन “अविचल”
राष्ट्रीय अध्यक्ष, मातृभाषा उन्नयन संस्थान
अणुडाक: arpan455@gmail.com
अंतरताना:www.arpanjain.com
[ लेखक डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’ मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा देश में हिन्दी भाषा के प्रचार हेतु हस्ताक्षर बदलो अभियान, भाषा समन्वय आदि का संचालन कर रहे हैं]
लेखक_परिचय-
डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मातृभाषा व साहित्यग्राम पत्रिका के संपादक व साथ ही, पत्रकारिता के विद्यार्थियों के शिक्षक डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’ मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु देशभर में हिन्दी भाषा के प्रचार, प्रसार और विस्तार के लिए निरंतर कार्यरत हैं।
आप कम्प्यूटर साइंस विषय से बैचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग (बीई-कम्प्यूटर साइंस) में स्नातक होने के साथ आपने एमबीए किया तथा एम.जे. एम सी की पढ़ाई भी की। उसके बाद ‘भारतीय पत्रकारिता और वैश्विक चुनौतियाँ’ विषय पर अपना शोध कार्य करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉ. अर्पण जैन ने 11 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हिन्दी में परिवर्तित करवाए, जिसके कारण वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्डस, लन्दन द्वारा आपको विश्व कीर्तिमान प्रदान किया गया।


