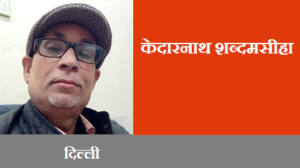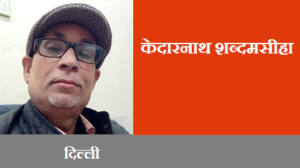Read Time7 Minute, 31 Second
आज जब दलित साहित्य पर नजर डालता हूँ तो पाता हूँ कि जैसे एक ठहराव आ गया है । अतीत का बहुत दोहराव हो रहा है । एक जो मानसिक फ्रेम बना हुआ है वह निकल नहीं रहा है । अधिकांश दलित साहित्यकार उन पुरानी परिस्थितियों से उबर नहीं पाये हैं । यही कारण है कि उसमें अभी भी दुख-दरिद्रता का अतिरेक दिखाई दे रहा है । परिस्थितियों का वर्णन ऐसा लगता है जैसे इतिहास को दोहराया जा रहा हो ।
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जाति और धर्म आज भी बड़ी समस्या हैं । खास तौर पर निम्न जाति वर्ग के लिए । जहां ये ग्रंथि उच्च वर्ग के मन में है वहीं यह हीनता की गांठ कहीं न कहीं निम्न वर्ग में भी अपनी गहरी जड़ें जमाये हुए है । अभी तक हमारा साहित्य सामंजस्य और नए आयाम इस जाति भेद को मिटाने के लिए नहीं दे पाया है । साहित्यिक एजेंडे में सिर्फ जाति ही नहीं होनी चाहिए । अगर इतिहास देखा जाय तो बहुत से उच्च वर्गीय चिंतकों ने भी जाति आधारित असमानता का विरोध किया है और समाज के सामने संघर्ष का रास्ता दिखाया है । आज के कहानीकारों की कथाओं में उत्पीड़न, दमन का अजेंडा तो मौजूद है मगर उस से बचने के विकल्प बहुत कम हैं । चिंतन का अभाव है । कहानी को मात्र किसी घटना की खबर होने से बचाने की सख्त जरूरत है । इस वजह से ऐसा लगता है जैसे दलित साहित्य वहीं खड़ा हुआ है जहां तीस-चालीस साल पहले खड़ा हुआ करता था ।
समाज में आए बदलावों को कलमबद्ध करने की जरूरत है । उस संघर्ष से आगे निकले हुए लोगों का हमने कहीं चित्रण नहीं किया । हमने कहीं उनको सम्मानित नहीं किया । हमने उन्हें समाज का आदर्श नहीं बनाया । जनचेतना के बजाय जातिचेतना को ज्यादा महत्व दिया । इसलिए मुझे प्रतीत होता है कि वर्तमान दलित साहित्य प्रगतिशील न होकर ठहराव का साहित्य बन गया है । साहित्यिक अंतर्विरोध कुछ साहित्यकारों द्वारा जानबूझकर पैदा किया जा रहा है । वस्तु स्थिति ये है कि निम्नवर्गीय जातियों ने इतने लंबे समय में भी अपने ही अंतर्विरोधों को पार नहीं किया है । आज भी उनमें आपस में संबंध और संवाद नहीं है । हमें सामाजिक बदलाव की तरफ बढ़ना होगा । इन अंतर्विरोधों के प्रति लड़ना होगा और इन्हे ऊर्जा देकर तेज करना होगा । इसके लिए आपसी एकता की दरकार है ताकि संघर्ष तेज हो सके । इस मुद्दे पर अंबेडकर , राहुल सांकृत्यायन , जोतिबा फुले को सामाजिक जीवन में उतारने की जरूरत है । रास्ता चलने से तय होता है मानचित्र बनाने से नहीं ।
वर्तमान राजनीति में दखल नहीं है। उनके नेता समाज से वोट लेते हैं , खुद को चमकाते हैं और मलाई खाने के लिए , सत्ता का सुख भोगने के लिए विरोधी पक्ष की शरण में ही दंडवत हो जाते हैं । जबकि वे वोट संघर्ष और बदलाव के नाम पर ही मांगते हैं । ऐसे नेता अपने ही लोगों का दमन करते हैं । क्या कारण है कि रूस की मजदूर क्रांति के बाद भी मजदूर, दलित,दमित इकट्ठा नहीं हो सके ? आर्थिक आजादी का फायदा व्यापारी और उद्धयोगपतियों ने उठाया । उद्धयोग की मूल ताकत मशीन के अलावा श्रमिक भी हैं । इस बात को इंगित नहीं किया गया । मशीनों का विरोध तो लक्ष्य रहा मगर मजदूरों की मजबूती कभी विकल्प नहीं बनी ।
क्यों मजदूर और किसान को भीख मांगनी पड़ती है ? क्यो वह कर्ज़ माफी के लिए गुहार लगाता है , ढ़ोक लगाता है ? क्योंकि उसने इस बात को सही से समझा ही नहीं कि उसके उगाये अन्न का कोई और विकल्प नहीं है । सामुदायिक संगठन बनाने की जरूरत । तुरंत फसल न बेचने का निर्णय जैसे कुछ हथियार हैं , जिस से व्यापारियों को किसान मिलकर मजबूर कर सकते हैं । कैसा अजीब मज़ाक है कि व्यापारी किसान के माल का दाम तय करता है , जिसने उगाया है वह फसल का दाम तय नहीं करता ।
आर्थिक कारण आज बहुत महत्वपूर्ण हैं । अर्थ ही सामाजिक बदलाब की ऊर्जा देता है । अंबेडकरवाद एक विकल्प है नया समाज बनाने के लिए । वह एक जीवन दर्शन है । जिन्होने रास्ता बंद किया वे रास्ता रोकना नहीं छोड़ सकते । वह उनका हक समझा हुआ है उन्होने , तब जिन्हें रास्ता बनाना है वे क्यों कमजोर हैं ? उनको भी संगठित होकर अपनी ताकत को प्रदर्शित और स्थापित करना होगा । बहुजन सिर्फ वोट नहीं है , मगर बिखराव होने से उसका महत्व भी बिखरा हुआ है । शासन में उसका दखल पैदा करना होगा । इस जाल को समझना होगा , काटना होगा और मुझे लगता है कि दलित, वंचित समाज को भी अपने चिंतकों को बार-बार अपने बीच बुलाकर उनसे संवाद करने की जरूरत है । जमीन के बदलाव पर निगाह रखनी होगी और समाज को हतोत्साहित करने वाली कथा-कहानियों से गुरेज करते हुए सकारात्मक सोच को रेखांकित करना होगा । इस संघर्ष में जातीय व्यवस्था को दरकिनार करते हुए सवर्ण गरीबों को भी बदलाव में साथ लेने की मैं हिमायत करना चाहता हूँ । वे भी इस दमन चक्र का शिकार हैं । एक दूसरे के सामने नहीं बल्कि एक-दूसरे के साथ मिलकर चलने की जरूरत है ।
दलित साहित्य में पुनर्चिंतन, नयी सोच के समावेश , समस्याओं के सकारात्मक हल , शिक्षा , संगठन और संघर्ष को पुनः स्थापित करने की जरूरत है । बिना लाठी-डंडे के भी , बिना खून बहाये भी क्रांति आ सकती है । इसलिए चिंतकों को समाज में आकर संवाद करने की जरूरत है और लोगों को भी जरूरत है कि वे उस पर अमल करें । बिना अमल ये चिंतन , ये किताबें , ये ग्रंथ सिर्फ रद्दी के ढेर हैं ।
#केदारनाथ शब्दमसीहा
दिल्ली
Post Views:
79