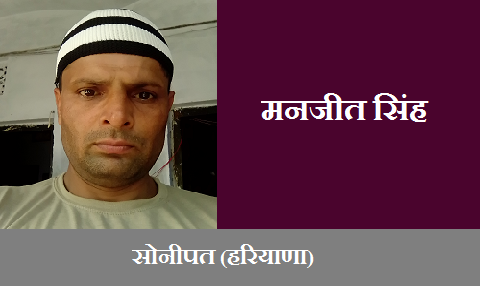
भारत में उर्दू भाषा का स्थान १९८१ की जनगणना में समग्र रूप से छठा है, जिसमें ३५ मिलियन से अधिक वक्ता हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर भारतीय राज्यों में केंद्रित हैं।
इस लेख का हिस्सा :
भारत में उर्दू भाषा का स्थान समग्र रूप से देश में छठा स्थान है। भारत में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक मातृभाषा उर्दू है। बोली जाने वाली भाषा के स्तर पर, उर्दू केवल मुसलमानों द्वारा हिंदी भाषा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है, लेकिन मुसलमानों द्वारा पसंद की जाने वाली लिपि फारसी अरबी है, जबकि व्यावहारिक रूप से सभी हिंदुओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिपि देवनागरी है। दो भाषाओं के साहित्यिक रूप भी अलग-अलग हैं, हिंदी लेखकों ने संस्कृत और उर्दू लेखकों को शब्दावली और शैली में फ़ारसी-अरबी स्रोतों से चित्रित किया है। 1947 में देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में संघ की एक आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू की अनदेखी की गई थी। उर्दू, जिसे स्वतंत्रता तक उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ने भी उस राज्य में अपना स्थान खो दिया। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 जिसमें हिंदी को राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। हालांकि उर्दू को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन यह केवल जम्मू और कश्मीर के छोटे से राज्य में एक आधिकारिक राज्य भाषा है।
पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़ी संख्या में घोषित उर्दू बोलने वालों के बावजूद, उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए 1960 और 1970 के दशक में शुरू किए गए विभिन्न संगठनों और आंदोलनों के माध्यम से मुस्लिम प्रवक्ताओं की मांग यूपी और बिहार के राज्यों के दोनों राज्यों में विरोध किया गया था। केवल 1980 के दशक में उर्दू को औपचारिक कानून के बजाय आदेश द्वारा दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था, बिहार के पंद्रह जिलों और यूपी के पश्चिमी जिलों में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, लेकिन बाद में यूपी अध्यादेश समाप्त हो गया। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में, १९८१ में १५.९३ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत के साथ प्राथमिक स्तर पर नामांकित केवल ३.६८ प्रतिशत छात्र उर्दू में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और १९७९-८० में माध्यमिक स्तर पर केवल ३.७९ प्रतिशत। प्राथमिक स्तर पर उर्दू में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या 352,022 थी। इसके विपरीत, कर्नाटक के आंकड़े ३६०,००९ थे और महाराष्ट्र के लिए ४३८,३५३, दोनों राज्यों में उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत कम मुस्लिम और उर्दू भाषी आबादी थी।
बिहार के विपरीत, उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी और उर्दू की स्थिति को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष इतना लंबा चला कि इस राज्य के अधिकांश लोगों ने अपनी मातृभाषा को हिंदी या उर्दू के रूप में घोषित कर दिया। 1961 मातृभाषा जनगणना। उदाहरण के लिए, हालांकि भोजपुरी भाषी क्षेत्र के बिहार की ओर उत्तर प्रदेश की ओर भोजपुरी भाषा के कई या अधिक देशी वक्ताओं की संभावना है, उत्तर प्रदेश में केवल 1, 20,119 भोजपुरी बोलने वालों की तुलना में 1961 में दर्ज किया गया था। बिहार में आठ करोड़ पंजाब में, आजादी से पहले शेष उत्तर भारत के विपरीत, हिंदी के प्रमोटर उस प्रांत में भाषा के लिए आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहे जहां आजादी तक अंग्रेजी और उर्दू आधिकारिक भाषा बनी रही। इस अवधि में, भाषा की मान्यता को लेकर सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्ष हिंदी और उर्दू की स्थिति को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच था। इस प्रतियोगिता में, हिंदुओं, जिनकी मातृभाषा पंजाबी थी, ने मुसलमानों और उर्दू पर संख्यात्मक लाभ हासिल करने के लिए हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित किया। अधिकांश मुसलमान, अपने हिस्से के लिए, वास्तव में विभिन्न पंजाबी बोलियाँ बोलते थे, हालाँकि उनके राजनीतिक नेताओं ने उर्दू के लिए आधिकारिक स्थिति को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी थी।
स्वतंत्रता के बाद, जिसमें पंजाब का विभाजन शामिल था, पूरी मुस्लिम आबादी का पाकिस्तान में प्रवास, और पश्चिमी पंजाब से पूरी सिख आबादी का भारतीय पंजाब में प्रवास, मान्यता के लिए संघर्ष तब हिंदी और पंजाबी के बीच एक हो गया।©
खान मनजीत भावड़िया
सोनीपत हरियाणा


